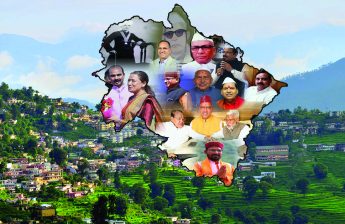राज्य पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 15 सालों में कुमाऊं के चार पवज़्तीय जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत के 283 गांव व तोक पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। लोग अपनी माटी से पलायन कर रहे हैं। घरों में ताले लटक चुके हैं। गांव के गांव खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों के गांव जो कभी अपनी खास पहचान रखते थे वह अब उनकी पहचान आपदा, पलायन व विस्थापन की रह गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यह मानते हैं कि यदि सीमांत के गांव खाली हुए तो सरहद की रक्षा करना बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि देश के इन प्रथम गांवों में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएं। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के माध्यम से योजना तो चल रही है लेकिन इसमें पूरे सीमावर्ती क्षेत्र कवर नहीं हो पा रहे हैं। देश के इन प्रथम गांवों का खाली होना सुरक्षा के लिहाज से भी खतरे की घंटी है। वर्ष 1971 के बाद से अब तक पुनर्वास व विस्थापन की नीति में अमल नहीं हो पाया है। जनपद पिथौरागढ़ में विस्थापन के लिए नए-नए गांवों की सूची तो लम्बी होती जा रही है लेकिन ग्रामीणों का विस्थापन नहीं हो पा रहा है
वर्ष 2025 को प्रदेश सरकार ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ घोषित करने की घोषणा कर चुकी है। इस घोषणा के तहत प्रदेश में 128 जनजाति बहुत गांव के लोग अपने गांव के विकास का खाका खुद खींचेंगे। यह सीमान्त के इन गावों के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है बशर्ते विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जमीनी धरातल पर उतर सकें। इस सुनहरी घोषणा के दूसरी तरफ विकास की बदरंग तस्वीर भी दिखाई देती है। राज्य पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 15 सालों में कुमाऊं के चार पवज़्तीय जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत के 283 गांव व तोक पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। लोग अपनी माटी से पलायन कर रहे हैं। घरों में ताले लटक चुके हैं। गांव के गांव खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों के गांव जो कभी अपनी खास पहचान रखते थे वह अब उनकी पहचान आपदा, पलायन व विस्थापन की रह गई है।
चीन सीमा से सटे उत्तराखण्ड के तीन जिले उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ के चार विकासखंडों के 11 गांव गैर आबाद हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन गैर आबाद गांवों को दोबारा बसाने की जरूरत है। इसके अलावा गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे कार्मिकों को आवासीय सुविधा मिले तो वह गांव में टिककर विकास योजनाओं को धरातल पर लागू कर सकें। रिपोर्ट कहती है कि जो सीमावर्ती गांव आबाद हुए हैं उनमें पिथौरागढ़ के गुमकाना, लूम, खिमलिंग, सांगरी, ढकधोना, सुम्तू व पोटिंग तो उत्तरकाशी में नेलांग, जडूंग के साथ ही चमोली में रेवलचक, कुरकुटी, फागती शामिल हंै। अभी अकेले पिथौरागढ़ के 97, चमोली के 29 व उत्तरकाशी के 10 गांव ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 किमी. की हवाई दूरी पर हैं। भूमि सुधारीकरण, जंगली जानवरों से सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी असुविधाओं के चलते ही इन गांवों से पलायन हुआ है। सीमांत क्षेत्रों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो विकास से कोसों दूर हैं।

देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यह मानते हैं कि यदि सीमांत के गांव खाली हुए तो सरहद की रक्षा करना बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि देश के इन प्रथम गांवों में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएं। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के माध्यम से योजना तो चल रही है लेकिन इसमें पूरे सीमावर्ती क्षेत्र कवर नहीं हो पा रहे हैं। जबकि सीमावर्ती गांव एक तरह से सुरक्षा प्रहरी की भूमिका भी निभाते हैं। सीमा पर होने वाली किसी भी तरह की हलचल की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से ही मिलती ह। लेकिन यही सीमावर्ती गांव पलायन के चलते अब खाली होने लगे हैं। देश के इन प्रथम गांवों का खाली होना सुरक्षा के लिहाज से भी खतरे की घंटी है। चीन व नेपाल की सीमा से उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिले के दजज़्नों गांव आते हैं इसमें से 51 गांव वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल हैं। अब कहा जा रहा है कि चीन व नेपाल सीमा से सटे 137 गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। इसमें से 51 गांव केन्द्र सरकार के वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम में तो वहीं 86 गांव राज्य सरकार विकसित करेगी। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना व मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत यहां पर विकास किया जाएगा। ये वे गांव होंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 से 15 किमी. के दायरे में है। अभी तक इस तरह के 11 गांव वीरान हो चुके हैं। दूसरी तरफ दर्जनों सीमावर्ती गांव आपदा की मार झेल रहे हैं। ये वर्षों से विस्थापन की बाट भी जोह रहे हैं। जिले के धारचूला तहसील के जुम्मा, जाराजिबली, मेतली, कनार, बरम, सुवा, धरपांगू, हिमखोला, छलमाछिलासों, गुगज़्वा, बुंगबुंग, जिप्ती, तांकुल, आदि गांव खतरे की जद में हैं। वर्ष 1971 के बाद से अब तक पुनर्वास व विस्थापन की नीति में अमल नहीं हो पाया है। जनपद पिथौरागढ़ में विस्थापन के लिए नए-नए गांवों की सूची तो लम्बी होती जा रही है लेकिन ग्रामीणों का विस्थापन नहीं हो पा रहा है। धारचूला का छलमा-छिलासू, हिमखोला, चामी (मेताली), जिमतड़ (कनार), छंग छंगरी (धर पांगू), न्यू धूरा (सुवा), बुंगबुंग का सिमखोला, अक्तू, रूमका सैन, कुजासू तोक, गगुर्व के स्यारी बांस (जम्कू- जुम्मा का भारभेली)। इन प्रभावित क्षेत्रों के भूगर्भीय सर्वेक्षण में पाया गया कि मुनस्यारी का टांगा, जोशा, धपा, धारचूला का जम्कू, धरपांगू, भाभेली, चामी, कटोजिया, तान्थर, चेतकला, ग्वालगांव, मोरी गांव रहने लायक नहीं रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला के 243 व मुनस्यारी के 137 परिवार रहने लायक नहीं हैं। इसके अलावा मालोपाती, सानीखेत, जुम्मा, साड़ा, गोल्पफा, नया बस्ती, आकोट, सिलौनी, धपा, जोशा, लोद, गैला, मेतली, छाना, कोट्यूड़ा, गोठी, बाता, हुड़की, कनार, बमनगांव खालसा, धरपांगू, रांथी, जम्कू, कुलथम, सेनर, तोमिक, तल्ला भैंसकोट, जिप्ती, हिमखोला, तांकुल, कनार, छलमाछिलासो सहित 37 गांवों का विस्थापन होना है। विस्थापन के नाम पर 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। जनपद पिथौरागढ़ का कुलथम गांव को आपदाओं का गांव कहा जाता है। आपदा यहां की नियति बन चुकी है। बार-बार यहां आपदा आती है। यहां 1999, 2004, 2008, 2009, 2013, 2014, 2018, 2020 में आपदा यहां तबाही मचा चुकी है। अब भी यहां 28 परिवार निवास करते हैं। भूगर्भीय सर्वेक्षण में इसे आपदा की जद में बताया गया है और यहां के लोगों का विस्थापन का जरूरी माना गया है। यहां के कई परिवार टिनशेड में रह रहे हैं।

किसी समय सीमांत का मिलम गांव जनपद पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा गांव माना जाता था। एक समय इस गांव में पांच सौ परिवार रहते थे। तब यहां की आबादी करीब ढाई हजार के करीब हुआ करती थी। ग्रामीण जमकर पशुपालन करते थे। साल में छह माह ग्रामीण गांव में व्यतीत करते थे। इस गांव से चार किमी दूरी पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थित है। अब मिलम गांव तक सड़क कट चुकी है लेकिन सवाल यह है कि क्या मिलम तक सड़क पहुंचने से इस गांव की तस्वीर बदलेगी। जबकि गांव खाली हो चुका है। हालांकि वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद पलायन के चलते वीरान हो चुके मल्ला जोहार के गांवों में अब-चहल पहल की उम्मीद की जा रही है। भारत-चीन युद्ध से पूर्व जोहार घाटी काफी समृद्ध मानी जाती थी। भारत-तिब्बत व्यापार अपने चरम पर रहता था। इसके अलावा जोहार घाटी के मतोलज़्ी, टोला, बुफूज़्, लास्पा, ल्वा, रिलकोट, गनघर, बिल्जू, खिलांच सहित कई गांव जड़ी-उत्पादन के लिए जाने जाते थे। भारत-चीन युद्ध व व्यापार खत्म होने से यहां से पलायन होना शुरू हुआ। मुनस्यारी-मिलम 65 किमी मोटर मार्ग कुमाऊं में चीन सीमा पर चौथी सड़क है। इससे पहले सीमा पर सोबला-दारमा मार्ग, तवाघाट- लिपुलेख सड़क व गुंजी-ज्योलिंगकॉग सड़क है।
इसी तरह साढ़े सात हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित गोल्फा गांव भी पलायन की मार झेल रहा है। इतिहासकार प्रो. गिरधर सिंह नेगी का मानना है कि करीब ढाई सौ साल पूर्व यहां भारी भूस्खलन हुआ था और यहां पर व्यापक क्षति हुई थी जिसमें कई ऐतिहासिक महत्व की चीजें दब गई थी। यह हिमालय क्षेत्र का समृद्ध गांव माना जाता है। गोल्फा गांव में आलू राजमा के साथ ही सेब का काफी उत्पादन होता है। यहां लोगों द्वारा पांच सौ नाली भूमि में कुटकी, अतीस, जटमासी, कूट, सतावरी व सालमपंजा आदि का उत्पादन भी किया जा रहा है। बताते हैं कि इस गांव में पहले करीब 10 मीटर लम्बी व 3 मीटर गहरी झील झील जो अब बरसाती नाले में तब्दील हो चुके हैं। सीमांत के गर्ब्याल गांव का भी यही हाल है। यह व्यास घाटी का गांव है। 10320 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसके समीप काली नदी बहती है। यह बहुत उपजाऊ इलाका रहा है। यह व्यास घाटी क्षेत्र का केंद्र बिंदु भी है। यह महर्षि व्यास की तपस्थली रहा है। यहां की सब्जियां व सेब बहुत प्रसिद्व हैं। कुल मिलाकर समय रहते सीमांत के गांवों में विकास को गति देना जरूरी है ताकि सीमा के ये प्रहरी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें।