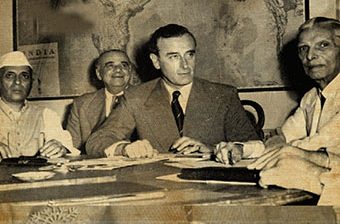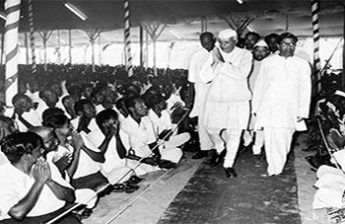भारत जैसे विविधता भरे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत यह मौलिक अधिकार हर नागरिक को दिया गया है कि वह अपनी बात, अपने विचार, अपनी कला बिना डर और दबाव के व्यक्त कर सके। मगर दुर्भाग्य यह है कि यह अधिकार सबसे ज्यादा चोटिल वहीं होता है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति की दुनिया में।
हाल में मलयालम फिल्म ‘जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल’ के साथ जो हुआ, उसने इस पुरानी बीमारी को एक नई मिसाल में बदल दिया। यह फिल्म एक बलात्कार पीड़िता के कानूनी संघर्ष पर केंद्रित थी। मगर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने इसे यह कहते हुए रोक दिया कि इसमें ‘जानकी’ नाम का इस्तेमाल है, जो एक पौराणिक चरित्र से जुड़ा है, और यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। बोर्ड ने इसे ‘असंगत और भड़काऊ’ करार दिया, खासकर यह देखकर कि इस नाम वाले पात्र से यौन हिंसा जुड़ी है और इसे दूसरे धर्म के अनुयायियों द्वारा अदालत में चुनौती दी जानी है।
बाद में कानूनी हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ, निर्माताओं ने नायिका के नाम का पहला अक्षर बदल दिया। मगर यह घटना केवल एक फिल्म या एक नाम तक सीमित नहीं है, यह इस बड़ी और गहरी समस्या की ओर इशारा करती है जिसमें कलात्मक स्वतंत्रता को बार-बार कुचला जाता है, कलाकारों को आत्म-सेंसरशिप की ओर धकेला जाता है और दर्शकों को यह तय करने का मौका ही नहीं मिलता कि वे क्या देखना, सुनना या समझना चाहते हैं।
सेंसर बोर्ड का काम केवल फिल्मों को ‘प्रमाणित’ करना है, यानी यह तय करना कि कौन सी फिल्म किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है- यू (सभी के लिए), यूए (सभी के लिए, मगर 12 साल से कम के बच्चों के लिए मार्गदर्शन आवश्यक), ए (केवल वयस्कों के लिए)। मगर व्यवहार में यह संस्था ‘नैतिक पहरेदारी’ और राजनीतिक दरबानी में बदल गई है।
हमारे सामने कई उदाहरण हैं, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का (2016), जिसे ‘महिला केंद्रित’ बताकर रोका गया, ‘पद्मावत’ (2018), जिसका नाम पद्मावती से बदलवाया गया और दर्जनों दृश्य काटे गए, ‘उड़ता पंजाब’ (2016) जिसमें 89 कट सुझाए गए थे। ‘एल2 : एंपुरान’ जिसमें केवल सम्भावित धार्मिक अपमान की आशंका में हस्तक्षेप हुआ। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि सेंसरशिप का असली कारण ‘जनहित’ या ‘कानून व्यवस्था’ नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के इशारे पर हर उस अभिव्यक्ति को रोकना है जो उनके एजेंडे से मेल नहीं खाती है।
अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो इंदिरा गांधी के समय की ‘आंधी’ (1975) को याद करना होगा, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित किरदार को लेकर इतना विवाद हुआ कि फिल्म का प्रसारण ही रोक दिया गया। ‘फायर’ (1996) समलैंगिकता के मुद्दे पर बनी एक साहसिक फिल्म थी, जिसे धार्मिक समूहों ने सिनेमाघरों में तोड़-फोड़ करके रोका। ‘वाटर’ (2005), जिसमें विधवाओं के जीवन पर सवाल उठाए गए, की शूटिंग ही रोक दी गई और निर्देशक दीपा मेहता को कनाडा जाकर फिल्म पूरी करनी पड़ी। ‘परजानिया’ (2005), जो गुजरात दंगों पर आधारित थी, को गुजरात में रिलीज ही नहीं होने दिया गया।
इसी तरह ‘किस्सा कुर्सी का’ (1977) में अमृत नाहटा ने संजय गांधी के नेतृत्व वाले राजनीतिक तंत्र पर व्यंग्य किया था। इमरजेंसी के दौरान इस फिल्म की सभी रीलें जला दी गईं। यह भारत में राजनीतिक सेंसरशिप की सबसे भयावह मिसाल है, और आज भी यह सवाल करती है कि क्या हम अपने ही लोकतंत्र के विचार से डरते हैं?
अब सवाल उठता है कि संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं, वे कहां चले जाते हैं? अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मगर अनुच्छेद 19(2) में ‘उचित प्रतिबंध’ की बात की गई है जैसे कि राज्य की सुरक्षा, शालीनता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था, अदालत की अवमानना, मानहानि। मगर अक्सर हम देखते हैं कि इन प्रतिबंधों की आड़ में अनुचित सेंसरशिप थोप दी जाती है।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने एस. रंगराजन वी.पी. जगजीवन राम (1989) मामले में स्पष्ट कहा था -“Freedom of expression cannot be suppressed on account of threat of demonstration and processions or threats of violence. That would tantamount to negation of the rule of law and a surrender to blackmail and intimidation.” (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदर्शन, जुलूस या हिंसा की धमकियों के कारण दबाया नहीं जा सकता। ऐसा करना कानून के शासन को नकारना और डर-धमकी के आगे समर्पण करना होगा।) मगर इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद, सेंसर बोर्ड, अदालतें और राज्य बार-बार उस पक्ष में झुक जाते हैं जो सबसे ऊंची आवाज में अपमान या अपवित्रता का दावा करता है। आज डिजिटल युग में नई चुनौती ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के रूप में सामने आई है। ‘तांडव’ (2021) जैसी वेब सीरीज पर राजनीतिक और धार्मिक आपत्तियां इतनी तेज हो गईं कि निर्माता को माफी मांगनी पड़ी और कथित आपत्तिजनक सीन हटाने पड़े। ‘काली पोस्टर’ विवाद में फिल्म रिलीज से पहले ही एफआईआर दर्ज हो गई। इंशाअल्लाह फुटबाॅल जैसी डाॅक्यूमेंट्री जो कश्मीर के युवाओं के सपनों और हकीकत को दिखाती थी, को राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बावजूद प्रमाणन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
सेंसरशिप का दूसरा पहलू दर्शकों के अधिकारों का हनन है। असल लोकतंत्र वह होता है जो अपने नागरिकों को यह मानकर चलता है कि वे परिपक्व हैं, निर्णय लेने में सक्षम हैं। मगर सेंसरशिप का रवैया नागरिकों को बच्चों की तरह ट्रीट करता है, मानो उन्हें तय करने की क्षमता ही न हो कि वे क्या देखें, क्या नहीं? जनता के नाम पर उठाई गई सेंसरशिप की तलवार, दरअसल, सत्ता, बहुसंख्यकवाद और रूढ़ीवाद के हितों की रक्षा करती है। यह रूढ़ीवाद ही तय करता है कि कौन-सी कहानी बताई जा सकती है, कौन-सी नहीं, किसका मजाक उड़ाया जा सकता है, किसका नहीं? किस पीड़ा पर फिल्म बन सकती है, किस पर नहीं?
अगर अंतरराष्ट्रीय संदर्भ देखें तो अमेरिका में ‘फ्री स्पीच’ का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रीढ़ माना जाता है। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि असहज करने वाले विचारों की भी रक्षा की जाएगी। यूरोप में भी हेट स्पीच (घृणा फैलाने वाले भाषण) और फ्री स्पीच के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची गई है। मगर भारत में ‘आहत भावनाओं’ का दायरा इतना बड़ा है कि लगभग कोई भी विचार सुरक्षित नहीं।
‘जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल’ मामले में जब केरल हाईकोर्ट ने पूछा- ‘‘क्या किसी ने इस नाम पर आपत्ति दर्ज की? किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं? क्या किसी ने वास्तव में आपत्ति दर्ज कराई है? और अब आप तय करेंगे कि निर्देशक किस नाम का प्रयोग करे और कौन सी कहानी बताए?’’ ये सवाल भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
कला का काम केवल मनोरंजन देना नहीं है, उसका काम असहज करना, झकझोरना, सोचने पर मजबूर करना भी है। एक परिपक्व समाज असहमतियों और जटिलताओं से भागता नहीं, उनका सामना करता है। कला में असहजता, असहमति और कटाक्ष को जगह देनी ही चाहिए, यही जीवंत लोकतंत्र की कसौटी है। सेंसर बोर्ड का काम केवल प्रमाणन तक सीमित होना चाहिए। कलाकारों को, चाहे वे फिल्मकार हों, लेखक हों, चित्रकार हों या संगीतकार, उनके विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हां, हिंसा भड़काने, घृणा फैलाने या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कंटेंट पर निश्चित ही रोक होनी चाहिए, मगर सम्भावित अपमान या अपवित्रता की कल्पना के आधार पर कला का गला घोंटना किसी सभ्य लोकतंत्र को शोभा नहीं देता।
एक मजबूत लोकतंत्र वह नहीं होता जो हर असहज सवाल को चुप करवा दे, वह होता है जो बहस और असहमति में भी अपनी शक्ति देखे। कलाकार, पत्रकार, लेखक और फिल्मकार लोकतंत्र के वो आईने होते हैं, जिनमें समाज अपनी सच्चाई देख सकता है। अगर हम उन पर परदा डालेंगे तो अंततः हम खुद अपने अंधकार में खो जाएंगे।
हालांकि वर्तमान काा सबसे बड़ा सच यही है कि असहज सवालों को लोकतंत्र का लोक उठा नहीं रहा है। कारण है धर्म और उसके बाद जाति की गोलबंदी जिसने लोक की चेतना को हर लिया है। जिन मूल्यों के साथ आजाद भारत की यात्रा शुरू हुई थी, वे मूल्य आज कि आर्थिक असमानता कहां पहुंच चुकी है, वह बेपरवाह है बढ़ते विदेशी कर्ज है, वह आंखें मूंदे बैठा है हर उस कटु सच से जो उसके हिंदू होने के आभासी गर्व को तोड़ता है। अंधकार बढ़ रहा है और देश का बहुसंख्यक खामोश है। सोचिए, ऐसे में क्या होगा लोकतंत्र का, देश का।