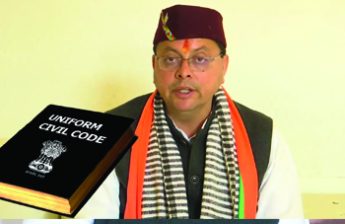देश की राजनीति पर 1989 के आम चुनाव के दौरान धार्मिक उन्माद पूरी तरह हावी हो चला था। भाजपा हिंदुत्व की अपनी अवधारणा को हिंदू वोटर के मन-मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए हर वह हथकंडा अपनाने में जुट गई थी, जिससे धार्मिक सौहार्द का वातावरण विषाक्त होने लगा और धार्मिक तुष्टिकरण की राह में सत्तारूढ़ कांग्रेस भी भाजपा के साथ होड़ लेने की कवायद में पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़ी थी। अक्टूबर, 1989 में राजीव ने कांग्रेस के चुनाव-प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की थी। उन्होंने यहां आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी के बाद ‘रामराज्य’ स्थापित किए जाने का वादा कर बहुसंख्यक मतदाता को लुभाने का प्रयास किया, तो इसके जवाब में भाजपा ने 9 नवम्बर के दिन विश्व हिंदू परिषद् के साथ मिलकर अयोध्या में ही राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम की घोषणा कर दी। विश्व हिंदू परिषद् बहुत पहले ही इस शिलान्यास कार्यक्रम की घोषणा कर चुका था लेकिन उसे ऐसा करने की इजाजत उत्तर प्रदेश की तत्कालीन नारायणदत्त तिवारी सरकार ने देने से इनकार कर दिया था। राजीव और उनके सलाहकार कांग्रेस के कोर वोट बैंक को भाजपा की तरफ आकर्षित होने से रोकना चाहते थे। नतीजा रहा विश्व हिंदू परिषद् को शिलान्यास की स्वीकृति मिलना। 9 नवम्बर के दिन बिहार के छोटानागपुर इलाके के एक दलित नवयुवक कमलेश्वर चौपाल के हाथों इस शिलान्यास कार्यक्रम करवाकर दक्षिणपंथी ताकतों ने भाजपा के पक्ष में दलित समाज को भी जोड़ने में आंशिक सफलता पाई थी।
नौवीं लोकसभा के लिए 22 से 26 नवम्बर, 1989 को वोट डाले गए। असम को खराब कानून-व्यवस्था के चलते चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। कुल 543 सीटों में से असम के शामिल न होने कारण 529 सीटों के लिए मतदान हुआ। कांग्रेस को इन चुनाव में 217 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 1984 में 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस चुनाव में मात्र 197 सीटें जीतकर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन केंद्र की सत्ता से उसे हाथ धोना पड़ा था। वी.पी. सिंह की अध्यक्षता वाले जनता दल को 143 तो 1984 में मात्र 2 सीटें पाने वाली भाजपा को 85 सीटों पर विजय हासिल हुई। दक्षिणपंथी राजनीति से घोषित तौर पर परहेज रखने वाले जनता परिवार ने सत्ता की चाह में वैचारिक विरोधियों के साथ समझौता करने में देर नहीं लगाई थी और भाजपा के बाहरी समर्थन से वी.पी. सिंह के नेतृत्व में ‘जनता की सरकार’ का केंद्र में गठन हो गया। भारतीय राजनीति में ‘मिस्टर क्लीन’ की छवि के साथ प्रचंड बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी मात्र पांच बरस के भीतर ही नाना प्रकार के आरोपों से घिरकर अपनी साख गंवा बैठे और सत्ता से बेदखल कर दिए गए।
एक सुखद स्वप्न का दुखद अंत
भारतीय राजनीति में राजीव गांधी का आगमन एक सुखद स्वप्न के समान था। पहली बार केंद्र की सत्ता आजादी के बाद की पीढ़ी के हाथों में आई थी। यह पीढ़ी अतीत के बोझ से मुक्त आधुनिक सोच वाली पीढी थी, जिसके कंधे पर देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी थी। 1984 के सिख-विरोधी दंगों को रोेक पाने में राजीव की विफलता के बावजूद वर्ष के अंत में हुए आम चुनाव में जनता जनार्दन ने उनके नेतृत्व पर प्रचंड आस्था जताई थी, लेकिन लोकसभा की 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस राजीव के नेतृत्व में एक के बाद एक भूल करती चली गई, जिसका नतीजा रहा 1989 में उसकी सत्ता से बेदखली। उनके शासनकाल के दौरान पंजाब, असम और त्रिपुरा में अलगाववादी गतिविधियों का विस्तार, रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार, पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका के आंतरिक मामलों में भारतीय सेना का हस्तक्षेप और 1987 का अकाल मुख्य तौर पर ऐसे कारण रहे, जिन्होंने राजीव गांधी की स्वच्छ छवि को प्रभावित करने का काम किया। राजीव प्रगतिशील सोच के उदारवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। राजनीति में उनका प्रवेश उनकी इच्छानुसार न होकर दबाव में लिया गया फैसला था। उनकी अनुभवहीनता और सत्ता के प्रति प्रारम्भिक उदासीनता उनके द्वारा लिए गए कई गलत फैसलों का कारण बनकर अंततः उनके और कांग्रेस के लिए रसातल में जाने का कारण बनी। राजीव सरकार ने पंजाब में हिंसा पर रोकथाम लगाने और अलगाववाद की भावना को थामने की नीयत से 1985 में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता जरूर किया, लेकिन उस समझौते को पूरी तरह लागू कर पाने में वह विफल रही। ‘खालिस्तान’ समर्थक आतंकवादियों ने संत लोंगोवाल की अगस्त, 1985 में हत्या कर इस समझौते की नींव हिलाने का काम किया तो केंद्र सरकार से राष्ट्रवादी सिखों की नाराजगी इस समझौते की तीन मुख्य बातों-चंडीगढ को पंजाब के हवाले किया जाना, 1984 के सिख दंगों की निष्पक्ष जांच और इन दंगों की जांच के लिए गठित रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों पर अमल न किए जाने के चलते तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा रहा पंजाब में आतंकी गतिविधियों का 1988, आते-आते अपने चरम पर पहुंच जाना। असम में लम्बे अर्से से चले आ रहे आंदोलन को राजीव गांधी के प्रयासों के चलते ही समाप्त किया जा सका था।
अगस्त, 1985 में असम के छात्र आंदोलनकारियों के साथ किए गए इस समझौते ने एक नई समस्या को जन्म देकर असम के कबीलाई इलाकों में हिंसा को विस्तार देने का काम किया। असम के आदिवासी बाहुल्य इलाके के मूल निवासियों ने खुद के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए एक बार फिर से राज्य में हिंसा पैदा करने का काम शुरू कर दिया था। पूर्वाेत्तर भारत के सातों राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में आदिवासी जनसंख्या बहुतायत में आजादी पूर्व से ही निवास करती आई है। इन आदिवासियों की एक जनजाति ‘बोडो’ कहलाती है। यह भारतीय संविधान की धारा 6 के अनुसार अनुसूचित जनजाति है। यह जनजाति तिब्बती-बर्मी भाषा-परिवार की एक शाखा है और भारत-मंगोल जातीय समूह (Indo & Mongoloid ethnic group) का हिस्सा मानी जाती है। असम की ब्रह्मापुत्र घाटी के उत्तरी क्षेत्र के चार जिलों- कोकराझार, दरांग, गोलपारा और कामरूप में यह जनजाति मुख्य रूप से वास करती है। बोडो खुद के लिए एक अलग राज्य की मांग आजादी पूर्व से करते रहे हैं। 1963 में नागालैंड के गठन के बाद इस मांग ने तेजी पकड़ी थी और बोडोभाषियों के हितों की बात करने के लिए एक राजनीतिक दल ‘प्लेन ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम’ (पीटीसीए) अस्तित्व में आया था। 1967 में बोडो छात्र संगठन ‘ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन’ का गठन किया गया। छात्र नेताओं ने पृथक राज्य बोडोलैंड की मांग को तेज करना शुरू कर दिया था। 1980 में असम आंदोलन, जिसकी कमान ‘ऑल असम स्टूडेंट यूनियन’ (आसू) के हाथों में थी, के साथ बोडो छात्र संगठन ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की थी। 1985 में राजीव सरकार के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ‘आसू’ नए राजनीतिक दल असमगण परिषद् का गठन कर राज्य में सत्ता हासिल करने में सफल रही। बोडो छात्र संगठन शुरुआती दौर में असमगण परिषद् के साथ मित्रवत् रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उनका मुख्य धारा के असमी राजनीतिक दलों के साथ मोहभंग होने लगा।1987 में ‘ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन’ ने अलग बोडोलैंड की मांग उठाकर हथियारबंद आंदोलन की राह पकड़ ली, जिसके चलते बोडो बाहुल्य इलाकों में हिंसा भड़क उठी। बोडो बाहुल्य जिलों में हड़ताल, रास्ता रोको आंदोलन जिसमें सड़क एवं रेलमार्ग को बाधित किया जाने लगा था और हिंसक घटनाओं ने भारी अराजकता पैदा करने का काम किया था। हालात इस कदर बिगड़े कि आए दिन असम में बम धमाके होने लगे थे, जिनमें कइयों की मौत हुई और करोड़ों की सम्पत्ति को जला दिया गया था। राजीव गांधी सरकार बोडो छात्र संगठन और असम सरकार के संग कई दौर की वार्ता के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई, जिससे उसकी छवि पर बुरा असर पड़ा था। हालांकि 1991 में एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के बाद इस समस्या का समाधान तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने निकालकर असम में शांति का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन तब तक राजीव इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। हैदराबाद विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर सुधीर जैकब जॉर्ज के अनुसार- ‘बोडो आंदोलन के मूल में अपनी विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखने की प्रबल भावना थी, जो असमियों द्वारा असम राज्य का पूरी तरह असमीकरण करने की अवधारणा के विपरीत थी… अपनी इस विशिष्ट पहचान को खोने का डर बोडो अशांति का मुख्य कारण था। पड़ोसी राज्यों मेघालय और नागालैंड में पहाड़ी जनजातियों की अपेक्षाकृत तरक्की और असम के दो पहाड़ी जिलों कार्बी और आंगलोंग तथा उत्तरी कछार क्षेत्र की जनजातियों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किए जाने के चलते भी बोडो नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इन जनजातियों से कहीं बड़ी आबादी होने के बावजूद असम सरकार द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया गया है… 1987 के बाद बोडो आंदोलनकारियों का सरकारी एजेंसियों द्वारा दमन और उन पर अनावश्यक बल-प्रयोग ने इस आंदोलन को उग्र करने का काम किया। असम सरकार ने ‘आतंक निरोधी’ कानूनों’ के अंतर्गत बोडो आंदोलनकारियों पर कार्यवाही करने और 3000 से अधिक एबीएसयू/बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में ले लिया था। इस प्रकार पूर्वाेत्तर, विशेष रूप से असम में केंद्र और राज्य सरकारों की असंतुलित नीतियों ने बोडो आंदोलन को तेज करने का काम किया। इसी दौर में केंद्र सरकार द्वारा मिजोरम के अलगाववाद संगठन ‘मिजो नेशनल फ्रंट’ के साथ समझौता (1986), त्रिपुरा के विद्रोही संगठन ‘त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स’ के साथ 1988 में समझौता और सबसे ऊपर, पश्चिम बंगाल में ‘गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट’ के साथ 1988 में शांति समझौता कर ‘दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल’ का गठन करने के चलते बोडो आंदोलनकारियों की अलग बोडोलैंड बनाए जाने की उम्मीद को हौसला दे डाला था।’
पश्चिम बंगाल के नेपाली भाषी पहाड़ी जिलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और इससे सटे दुआर क्षेत्र (पूर्वाेत्तर भारत का ब्रह्मापुत्र नदी के आस-पास का मैदानी इलाका जिसका कुछ हिस्सा जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिलों में आता है।) को अलग राज्य बनाने की मांग दशकों से यहां के गोरखा समुदाय द्वारा उठाई जाती रही है। 1980 में गोरखा ‘नेशनल लिबरेशन फ्रंट’ नामक संगठन ने अलग राज्य की मांग को हिंसक मार्ग के जरिए हासिल करने की मुहिम छेड़ दी थी, जिस कारण इस पूरे इलाके में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होकर इस पृथक राज्य के आंदोलन को अलगाववाद की तरफ ले गई। इस अतिवादी संगठन का नेतृत्व गोरखा नेता सुभाष धीसिंग के हाथों में था। 1986 से 1988 तक भीषण रूप से हिंसक हो चले इस आंदोलन में 1200 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था और अपने चाय बागानों के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ गई थी।
राजीव सरकार के प्रयासों के चलते अंततः 1988 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के मध्य दार्जिलिंग की पहाड़ियों को एक अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक ईकाई बनाए जाने पर सहमति बनी और दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल अस्तित्व में आई। पहला काउंसिल चुनाव जीतकर सुभाष धीसिंग इसके अध्यक्ष बने थे। हालांकि अलग गोरखालैंड बनाए जाने की मांग आज भी समय-समय पर उठती रहती है, लेकिन अब इसका असर लगभग समाप्त हो चला है। राजीव गांधी शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में इस समझौते का विशेष स्थान है। इसी प्रकार 80 के दशक में त्रिपुरा में भी अलगाववाद ने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। यहां ईसाई समुदाय के लोगों ने एक सशस्त्र संगठन ‘त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स’ की स्थापना कर अलग राष्ट्र की मांग उठानी शुरू की, जिसे स्थानीय आदिवासी समुदाय का भी समर्थन हासिल था। ईसाई मिशनरियों ने बेहद पिछड़े आदिवासी समूहों को आर्थिक मदद देकर उन्हें धर्म-परिवर्तन के लिए उकसाने का काम जमकर किया। 1988 में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद ‘त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स’ ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा की राजनीति को अपना लिया था।