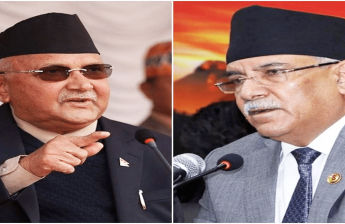राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक निर्णायक मोड़ ला दिया है। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक खींचतान ने जहां एक ओर वैश्विक मंदी की आशंका को जन्म दिया है, वहीं दूसरी ओर भारत जैसे देशों को एक रणनीतिक अवसर भी दिया है। यदि भारत इस अवसर को दूरदष्टि और तैयारी के साथ अपनाता है तो वह वैश्विक उत्पादन और निर्यात के केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है
अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी ‘अमेरिका फस्र्ट’ की नीति को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास किया है। उनकी टैरिफ नीति का मूल उद्देश्य अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना, व्यापार घाटे को कम करना और चीन की आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। यह नीति न केवल अमेरिका और चीन के व्यापारिक समीकरणों को प्रभावित कर रही है, बल्कि भारत सहित कई अन्य देशों के लिए अवसर और चुनौती, दोनों लेकर आई है।

राष्ट्रपति ट्रम्प का मानना है कि अमेरिका को लम्बे समय से वैश्विक व्यापार में नुकसान झेलना पड़ा है, विशेषकर चीन के साथ। व्यापार असंतुलन, बौद्धिक संपदा की चोरी, और सब्सिडी आधारित डंपिंग के खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया स्वरूप ट्रम्प प्रशासन ने चीन से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की है। कुछ मामलों में यह 145 प्रतिशत तक है। इनमें स्टील, एल्युमीनियम, स्मार्टफोन, बैटरियां, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर पैनल जैसी प्रमुख वस्तुएं शामिल हैं।
इस नीति के पीछ अमेरिकी घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, व्यापार घाटे को संतुलित करना, चीन को रणनीतिक और आर्थिक रूप से दबाव में लाना और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत तकनीकी क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को नियंत्रित करना है।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
हालांकि उद्देश्य सकारात्मक, लेकिन इसके व्यावहारिक प्रभावों ने कई स्तरों पर चिंता बढ़ाई है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे अमेरिकी जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय है। खासकर टेक्सटाइल और इलेक्ट्राॅनिक्स सेक्टर में कीमतों के कारण सेकंडहैंड बाजार तेजी से बढ़ रहा है। कई अमेरिकी कम्पनियों को चीन में उत्पादन जारी रखने और विकल्प ढूंढ़ने के बीच संतुलन बनाना कठिन हो रहा है और वे भारत समेत अन्य देशों की तरफ रुख करने लगी हैं।
चीन पर प्रभाव और रणनीतिक जवाब
अमेरिका की टैरिफ नीति से चीन के निर्यात को सीधा झटका लगा है। अमेरिका, जो चीन के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, वहां मांग घटने लगी। इसके परिणामस्वरूप चीनी उत्पादन पर असर पड़ा और रोजगार के अवसरों में गिरावट आई है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन छोड़कर वियतनाम, भारत और मैक्सिको जैसे देशों की ओर रुख करना शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे अमेरिका से निर्यात आने वाले दिनों में खासा कम होना तय है। चीन अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में नए व्यापारिक साझेदार खोजने में सक्रिय हो गया है।
भारत के लिए अवसर और चुनौतियां

चीन से बाहर जा रही कंपनियों के लिए भारत एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरा है। एप्पल समसैंग और फाॅक्सकान जैसी कंपनियों ने भारत में निवेश बढ़ाया है। भारत से अमेरिका को निर्यातित स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्राॅनिक्स, चीन की तुलना में 20 प्रतिशत सस्ते हो सकते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्ृंखला में विविधता लाने की रणनीति के तहत भारत को नई भूमिका मिल सकती है।
हालांकि यहां यह गौरतलब है कि भारत की लाॅजिस्टिक, ऊर्जा आपूर्ति और कानूनी प्रक्रियाएं अब भी वैश्विक मानकों से पीछे हैं। जटिल श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं और अप्रत्याशित कर नीति निवेशकों के लिए बाधा बन सकती हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश भी उत्पादन हब बनने की होड़ में हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर का मत है कि भारत को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए संरचनात्मक सुधारों और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम करना होगा।
विश्व व्यापार में हो रहे इस बड़े बदलाव के बीच भारत यदि अपने औद्योगिक सुधारों को गति देता है, निर्यातोन्मुख नीतियां बनाता है और वैश्विक निवेशकों के लिए वातावरण को सरल बनाता है तो वह एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकता है। भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभ, डिजिटल ताकत, और नीति समर्थन की सम्भावना है – जरूरत है तो केवल समन्वित और निर्णायक कार्रवाई की।