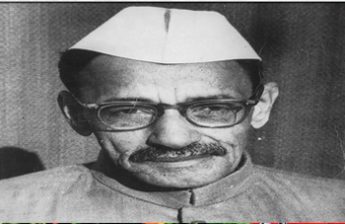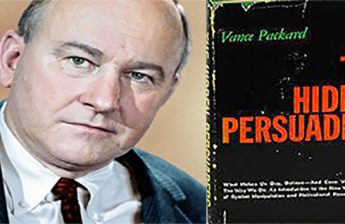हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुके हैं जहां भारत के संविधान की आत्मा, समाज के बुनियादी ढांचे और धार्मिक-सामाजिक चेतना के बीच निरंतर टकराव हो रहा है। संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है लेकिन जमीनी हकीकत बार-बार यह साबित करती है कि समाज में न तो समानता है, न आर्थिक न्याय, न ही धार्मिक समरसता। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में यादव समाज के युवाओं द्वारा की गई कथा वाचन और पूजा-पाठ की घटनाओं को जिस प्रकार अपमान और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, उससे इस देश में आज भी जातिगत श्रेष्ठता की गहरी जड़ों का काला सच सामने आता है। इन युवाओं के बाल काटे गए, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। और यह सब इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा कर्मकांड किया जिसे आज भी कुछ विशेष जातियां केवल अपने अधिकार का क्षेत्र मानती हैं।
यह कोई छिटपुट सामाजिक हिंसा नहीं है, बल्कि यह भारत की धार्मिक सत्ता संरचना की पुनर्पुष्टि है, जिसमें पूजा-पाठ, भजन, कीर्तन, मंदिर, पुरोहिताई जैसे सारे धार्मिक कर्मकांड कुछ जातियों के वर्चस्व का क्षेत्र माने जाते हैं और जब पिछड़ी जातियों के लोग, विशेष रूप से यादव, कुर्मी, जाटव, पासी जैसे समुदाय, इन मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो हिंदुत्व के पैरोकारों को यह असहज कर देता है। वे इस असहजता को परम्परा और पवित्रता के नाम पर ढंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मूल स्वरूप सामाजिक वर्चस्व की पुनरावृत्ति ही होता है।
इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी हस्तक्षेप किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि यह घटना धर्म के नाम पर जातिगत वर्चस्व की मानसिकता को दर्शाती है, और यह बताती है कि पूजा-पाठ और धर्म कर्म के मंच को अभी भी एक विशेष वर्ग की जागीर बनाए रखने की प्रवृत्ति समाज में गहराई से मौजूद है। उन्होंने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर यह आरोप भी लगाया कि वे कथावाचन के लिए ‘अंडर द टेबल’ भारी धनराशि लेते हैं, जबकि जब यादव समाज का कोई युवक कथा कहता है तो वह अपमान और बहिष्कार का पात्र बनता है। धीरेंद्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें सनातन धर्म से नहीं, बल्कि उनकी लोकप्रियता से कुछ लोगों को दिक्कत है, और यह आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। यह टकराव दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का प्रतीक है- एक वह जो धर्म को ब्राह्माणवादी अनुशासन की परिधि में रखना चाहती है और दूसरी जो उसे जनसामान्य का अधिकार मानती है।
इस विमर्श को और गहरा बनाता है कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पन्न विवाद, जिसमें कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने यह मांग की कि गैर-हिंदू होटल, दुकानदार, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर देवी-देवताओं की तस्वीरें न लगाएं और स्पष्ट रूप से बताएं कि वे किस धर्म के हैं। यह मांग न केवल संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विरुद्ध है, बल्कि यह धार्मिक बहिष्कार और सामूहिक शक की संस्कृति को जन्म देती है। क्या भारत अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां किसी व्यक्ति का व्यवसाय उसके धार्मिक प्रमाणपत्र पर निर्भर करेगा? क्या पंथनिरपेक्षता अब केवल एक किताब का शब्द रह जाएगी?
इसी संदर्भ में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल को प्रस्ताव दिया है कि वे उन्हें महागठबंधन (इंडिया ब्लाॅक) में शामिल करें, ताकि मुस्लिम वोटों का बिखराव रोका जा सके। ओवैसी का तर्क है कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक न समझा जाए, बल्कि नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी में भी स्थान दिया जाए। उनका संकेत स्पष्ट है कि विपक्ष यदि गम्भीर है तो उसे ‘साझा मंच’ की कल्पना को व्यवहार में उतारना होगा। इसके जवाब में कांग्रेस और राजद जैसे दल इस प्रस्ताव से झिझकते नजर आए हैं। कारण है, भाजपा इसका प्रचार मुस्लिम तुष्टिकरण के रूप में करेगी और इसका राजनीतिक लाभ उठाएगी।
यही वह संदर्भ है जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि ‘‘भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति नहीं करती।’’ यह बयान राजनीतिक पाखंड का स्पष्ट प्रतीक है। जब भाजपा की राजनीति राम मंदिर, काशी काॅरिडोर, गंगा आरती, महाकाल लोक, कांवड़ यात्रा और हिंदुत्व के सांस्कृतिक अभियान से संचालित होती है, जब प्रधानमंत्री खुद मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करते हैं तो यह दावा कि
भाजपा धर्म आधारित राजनीति नहीं करती बेहद हास्यास्पद है। रिजिजू का यह कथन दरअसल ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम नेतृत्व को ‘धर्म आधारित राजनीति’ के नाम पर संदेह के घेरे में लाकर बहुसंख्यक वोट को और गोलबंद करना है।
इसी के साथ, महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता आंदोलन के तहत हिंदी विरोध भी एक बार फिर उभरकर सामने आया है। मराठी को सांस्कृतिक अस्मिता और क्षेत्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बनाया जा रहा है और हिंदी भाषियों को बाहरी करार दिया जा रहा है। यह परिघटना भारत के भीतर मौजूद भाषाई टकरावों की गहराई को उजागर करती है। एक ओर हम ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की बात करते हैं, दूसरी तरफ भाषाओं के नाम पर नागरिकों को टुकड़ों में बांट देते हैं।
उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का हालिया बयान इस पूरे विमर्श को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ‘‘पंथनिरपेक्ष’’ और ‘‘समाजवादी’’ जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। यह मांग केवल विचारधारात्मक बहस नहीं है, यह उस सामाजिक समझौते पर सीधा आघात है जो भारत को एक लोकतांत्रिक, समावेशी और धर्म-तटस्थ राष्ट्र बनाता है। ‘‘पंथनिरपेक्ष’’ शब्द यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा और ‘‘समाजवादी’’ यह दर्शाता है कि संसाधनों का वितरण न्याय संगत होगा। इन शब्दों को हटाने की बात करना संविधान की आत्मा को काटने जैसा है।
इन सारे विमर्शों के मूल में वही प्रश्न बार-बार गूंजता है, जिसे डाॅ. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Annihilation of Caste (1936) में उठाया है। इस पुस्तक में अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है कि “The real problem is not that religion is bad. The real problem is that religion has been perverted and that it has been used to serve the interests of a class.” (असल समस्या यह नहीं है कि धर्म बुरा है। असली समस्या यह है कि धर्म को विकृत कर दिया गया है और उसे एक विशेष वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।)उन्होंने यह भी कहा है कि “I am sorry] I will not have faith in a religion which cannot recognize the equality of human beings.” (मुझे खेद है, मैं उस धर्म में आस्था नहीं रख सकता जो मनुष्यों की समानता को नहीं मानता।) अम्बेडकर का यह नैतिक विद्रोह केवल धार्मिक सत्ता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता के विरुद्ध भी है जो भक्ति, धर्म और पवित्रता के मंच पर भी असमानता को बनाए रखना चाहती है।
अम्बेडकर के इस चिंतन को और आगे बढ़ाया डाॅ. राममनोहर लोहिया ने, जिन्होंने 1960 के दशक में ‘‘पिछड़ा पावे सौ में साठ’’ का नारा दिया था। उनका आशय पिछड़ी जातियों से था, जिनकी जनसंख्या 60 प्रतिशत से अधिक है, को शासन, प्रशासन, शिक्षा, धर्म और अर्थव्यवस्था के हर मंच पर 60 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। डाॅ. लोहिया का मानना था कि ‘‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी।’’ यह सिर्फ आरक्षण की मांग नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र को समाज के हर स्तर पर समानता और सहभागिता की दिशा में ले जाने की नीति है।
आज जब यादवों को कथा कहने पर सजा दी जाती है, जब दलितों को मंदिरों में प्रवेश पर रोका जाता है, जब पिछड़ों को धर्म-चर्चा से बाहर रखा जाता है, तब यह स्पष्ट होता है कि न तो अम्बेडकर का ‘जाति का उच्छेदन’ हुआ है, न ही लोहिया की ‘समान भागीदारी’ सम्भव हो सकी है। राममनोहर लोहिया ने यह भी चेतावनी दी थी कि बढ़ती आर्थिक असमानता भारत के लिए घातक सिद्ध होगी। आज की स्थिति में यह चेतावनी और अधिक अर्थवान हो गई है। आज भारत की 10 प्रतिशत आबादी राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत नियंत्रित करती है, जबकि निचले 50 प्रतिशत को महज 13 प्रतिशत आय मिलती है। समाज के भीतर यह आर्थिक विभाजन केवल संसाधनों का नहीं, बल्कि अवसरों, पहचान और गरिमा का विभाजन भी है।
धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक संरचना, ये सब एक ही सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलू हैं। जब इन पर असमानता का वर्चस्व होता है, तब लोकतंत्र केवल सत्ता पाने का माध्यम, नागरिकता एक पहचान पत्र और संविधान एक प्रतीक बन रह जाता है।
अब समय आ गया है कि हम भारत के संविधान को केवल दीवार पर लटकाई गई तख्ती नहीं, बल्कि एक जीवंत सामाजिक दस्तावेज की तरह देखें। अम्बेडकर और लोहिया की चेतावनियों को सिर्फ इतिहास की बात नहीं, आज की आवश्यकता की तरह समझें। यदि भारत को सच में अखंड बनाना है तो उसकी विविधता को समानता के सूत्र में बांधना होगा। वरना हम भले ही नक्शे पर एक देश रहें, समाज और चेतना में हम लगातार बंटते रहेंगे।