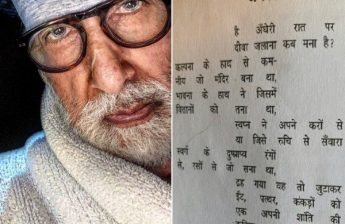- प्रज्ञा पाण्डेय
साहित्यकार एवं स्त्री विषयों पर लेखन
ललित मोहन जोशी निर्देशित फिल्म ‘अङ्वाल’ जो कुमाऊंनी भाषा के महानतम कवियों को याद करने के बहाने मातृभूमि के प्रति उत्कृट प्रेम का एक उदगार भी है।
कुमाऊंनी भाषा में अङ्वाल शब्द का अर्थ होता है आलिंगन। यह कई मनोभावों में बसता है फिर भी इसकी भावभूमि नेह और नाता ही है। आप जिससे नेह करते हैं उसे अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। ‘अङ्वाल’ फिल्म में ललित मोहन जोशी अपनी मातृभूमि कुमाऊं को अपने हृदय से लगाते हैं। इस तरह फिल्म का नाम अङ्वाल (आलिंगन) अपने अर्थ के सुन्दरतम विस्तार को पाता है।
फिल्म के पहले दृश्य में ही निर्देशक कहते हैं ‘कुमाऊं , मेरी मातृभूमि’ तब उनके शब्दों की संवेदना, मातृभूमि से बिछुड़ने की उनकी पीड़ा और दूर जा बसने की उनकी वेदना उनकी आवाज में उतरती है। जैसे बच्चा मां को पुकारता है। हिमालय की गोद में फैली पहाड़ियां प्रतिध्वनि के रूप में उन्हें जवाब देती हैं कि उन पहाड़ों के पास भी उनको छोड़कर जाने वालों के लिए उतनी ही वेदना है। इस तरह की फिल्में पहले ही दृश्य में बांध लेती है।
ललित मोहन जोशी जो नैरेटर की भूमिका में भी हैं, कहते हैं कि वे अपनी मातृभूमि छोड़कर हजारों मील दूर लन्दन जा बसे लेकिन पहाड़ों की खुशबू उनके भीतर आज तक बसती है। दर्शक भी अपने किसी ऐसे ही बिछोह की स्मृति से भर उठता है।
यह फिल्म कुमाऊंनी भाषा में बनी है जिसमें सब टाइटल्स अंग्रेजी भाषा में हैं। भाषा से अपरिचित होते हुए भी आप सब-टाइटल्स नहीं पढ़ना चाहते हैं और भावों को कहती भाषा को सुनने के लिए अपने कानों को सजग करते हैं। संवाद के लिए भाषा से बड़ी भूमिका उस मन की होती है जो भावनाओं से भरा है। फिल्म में ललित मोहन जोशी का नरेशन यह सिद्ध करता है कि इस दुनिया में शब्दों की भाषा को जानना उतना जरूरी नहीं जितना मन की भाषा को महसूस करना जरूरी है।
फिल्म के भाव-दृश्यों को देखते हुए मुझे रसूल हमजातोव की पुस्तक ‘मेरा दागिस्तान’ की याद आती है। हमजातोव को भी अपने दागिस्तान से ऐसा ही प्यार है कि वे उसके बारे में विह्वल होकर, भावों से भरकर लिखते हैं। रसूल हमजातोव अपने देश के छोटे-छोटे किस्से, छोटी-छोटी कहानियां और घटनाएं लिखते हैं। उसे बार-बार ‘मेरा देश दागिस्तान’ कहते हैं।
अङ्वाल में नैरेटर कहते हैं ‘मेरे मामाओं की और मेरी मां की भूमि। उनकी जन्मभूमि और उनकी काव्य भूमि।’ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का एक दृश्य है। स्टेशन पर कुछ देर रुक कर ट्रेन जाने लगती है। जाती हुई ट्रेन कुछ देर तक दृश्य में रहती है और आप उदास होते हैं। स्टेशन पर सभी अपरिचित हैं लेकिन बिछोह का एक भाव उभरता है। फिल्म में यह भाव आपको व्याकुल करता है। एक घंटे सत्रह मिनट की यह फिल्म कुमाऊं के महानतम कवियों की स्मृति और पहाड़ों से पलायन की एक उदास धुन की तरह है।
कुमाऊंनी भाषा के कालजयी कवियों को ललित मोहन जोशी इस फिल्म के माध्यम से दुनिया के सामने ले आते हैं और मातृभूमि से प्रेम का संदेश भी देते हैं। कालजयी कविताओं के माध्यम से वे पहाड़ों के संघर्षपूर्ण जीवन से परिचित कराते हैं। फिल्म में संवाद करते समय, निर्देशक अपने ननिहाल, अपने बचपन के स्कूल, बीते समय को, कवियों की स्मृतियों को और उनकी कविताओं पर बहुत से लोगों से बातें करते हुए अनेक तथ्य लेकर आते हैं। कवितायें जो ब्रिटिश काल से वर्तमान समय तक फैली हैं। ललित मोहन जोशी अपनी ननिहाल मालौंज जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने बचपन को ढूंढता उन्हीं रास्तों की हर शै को छूने की उत्कट चाह रखता हो और वह सब समेट लेना चाहता है जो छूट गया है।
हमारे पूर्वांचल में ननिहाल को ननिऔरा कहते हैं। ननिऔरा वह जगह होती है जहां मां का बचपन बीता होता है। किसी बच्चे की स्मृति में मां का घर मां से कम नहीं होता। पहाड़ के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से जाते ललित मोहन जोशी के ननिहाल के उस घर की एक दीवार भर बची है घर गिर चुका है जिस घर ने उनके दो मामाओं को कविता लिखने की प्रेरणा दी थी। वे उसे छूते हैं और भारी कदमों से लौटते हैं। यहां फिल्म वैश्विक संवेदना से जुड़ती है। हम सब यूं ही लौटते हैं अपने उन गांवों से जहां हमें अपना कुछ भी बचा हुआ नहीं मिलता।
फिल्मकार ललित मोहन जोशी अपने पैत्रिक गांव शिलौटी, नौकुचियाताल में वर्षों से उपेक्षित वीरान पड़े अपने घर लौटते हैं जहां दरवाजे पर लगा ताला भी बहुत पुराना हो गया है। स्मृतियों से भरे कमरे जो वर्षों से बंद पड़े हैं। एक स्कूल, जहां एक बचपन छाता लेकर चुपचाप पहुंचता है। निर्देशक को याद आता बचपन का स्कूल जहां आज के बच्चे बैठे हुए सरस्वती वंदना गा रहे हैं – तू हमारी ज्ञान देवी हम तेरे पुजारी। मैय्या हंस की सवारी।
‘अङ्वाल’ कुमाऊं क्षेत्र के आठ कवियों के जीवन और स्मृतियों को समेटती हुई उनकी कविताओं, गीतों और उनके जीवन के बारे में बताती है। इस फिल्म का अद्भुत फिल्मांकन, कानों को मधुर लगता पहाड़ी संगीत और पहाड़ी धुन, नदी और पनचक्की के दृश्य आपको शाश्वत जीवन और काल चक्र से जोड़ते चले जाते हैं। वनों की हरियाली, उनके खेत और नदियां, पतले रास्तों, सीढ़ीनुमा खेतों और छोटे-छोटे घरों से होकर गुजरता संगीत हृदय में समा जाता है।
पहाड़ों का जिक्र हो और बुरांश के फूलों का जिक्र छूट जाए यह किसी तरह सम्भव नहीं है। बुरांश के फूलों पर सुमित्रानंदन पन्त की कुमाऊंनी में लिखी एकमात्र कविता है उसका बहुत ही भावपूर्ण पाठ आप फिल्म में सुनते हैं। इस तरह अनजानी भाषा मन को छूती है। कविता को फिल्म में ध्वनि और दृश्य के माध्यम से अद्भुत रूप में फिल्माया गया है इस तरह कि स्क्रीन पर फैले बुरांश के जलते हुए लाल रंग को दर्शक महसूस करते हैं। फूलते हैं बुरुंश तो जंगल जैसे जल जाएं। पहाड़ी फूल बुरुंश पर सुमित्रा नंदन पन्त की कविता- ‘सार जंगल में त्वे जस क्वे न्हां रे, क्वे न्हां, खिलन छै कै बुरुंश जंगल जस जलि जा, सल्ल छ, दयार छ, पई, अयांर छ, सबनाक फागन में पुंगनक भार छ, पर त्वी में दिलै कि आग, त्वी में छ जवानिक फाग, रगन में नई ल्वे छ प्यारक खुमार छ। कवि श्यामाचरणदत्त पन्त जो लिखने के लिए लोगों को और परिवार की स्त्रियों को भी प्रेरित करते थे उनकी एक कविता घट और ताल की धुन और संगीत के साथ उसका फिल्मांकन बहुत ही मार्मिक है। नदियों के किनारे बसने वाली हमारी सभ्यता में नदी के गीत शाश्वत और कालजयी हैं। ‘बीच ताल में नौ ऐ गे रे थक ने चला, चला पतवार।’ कुहासा है लेकिन तुम धीरज रखना नाविक, तुम नदी-जल को पार कर जाओगे।
उत्तरा सुकन्या जोशी की मधुर आवाज दृश्य में बहती नदी में गहरे उतर जाती है। दृश्य और आवाज किसी क्लासिक फिल्म का सुंदर दृश्य रचते हैं और कई मांझी गीत आंखों में साकार हो जाते हैं।
इस फिल्म में कुमाऊंनी भाषा के एक और कवि लोक रत्न पन्त ‘गुमानी’ (1791 – 1846) की चर्चा है, जो लगभग दो सौ बीस (220) साल पुराने हैं और कुमाऊंनी के आदि कवि हैं। फिल्म में इस कालजयी कवि की उपेक्षा के दर्द भी उभरते हैं। साहित्य ने उन्हें उस तरह जगह नहीं दी जिसके वे हकदार थे फिर भी उन पर अनेक तथ्य पुरानी पत्रिकाओं और किताबों में मिलते हैं, फिल्म इस बात की चर्चा करती है। फिल्म में काफल एक पहाड़ी फल पर उनकी एक कविता का सुंदर पाठ है। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में बहुत कविताएं लिखी हैं। वे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पचास साल पहले से लिख रहे थे। फिल्म बताती है कि उन्हें खड़ी बोली का पहला कवि कहा जा सकता है।
फिल्म विस्मृति में खो चुके कवियों को उनकी कविताओं के साथ पुनर्जीवन देती है। कवयित्री दिवा भट्ट कहतीं हैं कि हमारे अल्मोड़ा से जाने कितने लेखक हिंदी भाषा में गए। वे हिमांशु जोशी, इला चन्द्र जोशी, मनोहर श्याम जोशी। शैलेश मटियानी, ताराचंद पाण्डेय और अनेक लेखकों और कवियों को याद करती हैं। वे कहतीं हैं हमारी अल्मोड़ा की भूमि ऊर्जा से भरी है। कवि गौरी दत्त पाण्डेय को बहुत शिद्दत से याद करती है जिन्हें लोग गौरदा के रूप में जानते हैं।
शेखर पाठक कहते हैं कि गौरदा ने छोटे-छोटे विषयों पर कविताएं लिखी हैं। कुछ भी छोड़ा नहीं। उनकी कविताओं में जाने कितना इतिहास मिलता है। चाय जिसका ब्रिटिश राज में परिचय कराया जा रहा था और तब मुफ्त में पिलाई जा रही थी। उस पर उनकी कविता वापस उन्हीं दिनों में ले जाती है। शेखर पाठक इतिहासकार और ‘पहाड़’ पत्रिका के सम्पादक हैं। छाते पर, तकली पर, गिलास पर, दातुन पर, गांधी पर, उन्होंने कविताएं लिखीं। फिल्म में कवि त्रिभुवन गिरी गौरदा को बहुत मन से याद करते हैं। ‘ओह भाभी कैसे छोडूं ये चाय मुझे इसकी लत लग गयी है।’ ऐसी ही उनकी कई कविताओं की बात करती है फिल्म।
गौरदा का समय 1872 – 1939 का है। उनकी 1926 की लिखी कविता चिपको आन्दोलन में बेहद सामयिक सिद्ध होती है और याद की जाती है। सच्ची कविता शाश्वत होती है और कभी नहीं मरती। फिल्म बताती है कि गौरदा कुमाऊंनी के उच्च कवि-शिखर हैं। देव सिंह पोखरिया जो आज के कवि हैं, की एक कविता ‘धौसिया ठोक दे निसान’, एक महत्वपूर्ण रचना है जो पहाड़ में जगार की चेतना जगाने वाली कविता है जिसका सांस्कृतिक महत्त्व है। फिल्म पहाड़ों से पलायन की बात को बेहद संजीदगी से कहती है। उजड़े हुए तमाम घर हैं, टूटी छतों के मकान हैं जिनको देखने भी अब कोई नहीं आता। पलायन विश्व व्यापी समस्या है।
फिल्म अपने अंत की ओर बढ़ती है, कवि श्यामाचरणदत्त पन्त की कविता ‘घट’ के दर्द भरे फिल्मांकन से। इसमें हम जीवन के तमाम ताने बाने को देखते हुए जीवन के शाश्वत सत्य और यथार्थ को देखते हैं। कविता कहती है कि कालचक्र की पनचक्की चलती रहती है जिसमें दिन और रात पिसते रहते हैं। किसी का जन्म और किसी की मृत्यु होती है। एक पल में जीवन का दाना पिस जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन चक्र में बस रात-दिन पिसना रह जाता है। इस गीत के साथ पनचक्की के दृश्य, गेहूं के दानों का पिस कर पिसान होना, झरने, नदी और पहाड़ सभी बार- बार आते हैं। कमला पांडे की आवाज में गाया गया यह गीत बहुत मर्मस्पर्शी है। अपने दादा की इस कालजयी कविता का जिक्र फिल्म में पहले दिवाकर पन्त करते हैं जिन्होंने अपने दादा की कविता की विरासत को संभाल कर रखा हुआ है। श्रीमती सरोज पन्त भी अपने ससुर कवि के बारे में बहुत सी बातें बताती हैं, श्रीमती विनता पांडे ने भी अपने कवि पिता रामदत्त पन्त की एक कविता को फिल्म में गाया है, इन सब के चित्र क्रमशः आते-जाते हैं जो वर्ष 2020 से 2022 के बीच इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गए हैं। कविता निर्गुण भाव में आकर सूफियाना हो गई है।
पहाड़ तो यों भी सौन्दर्य का शिखर होते हैं उसमें रंगोली अग्रवाल के अद्भुत फिल्मांकन ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं। हरीश चंद्र पन्त और चंद्रशेखर तिवारी के निर्देशन में, सरोद वादक स्मित तिवारी और बांसुरी वादक नितेश बिष्ट ने पहाड़ी धुनों को अद्भुत संगीत में पिरोया है। सरोद और तबले के साथ बांसुरी की धुन मोह लेती है। फिल्म में सब टाइटल्स और रिसर्च का काम कुसुम पन्त जोशी जी ने किया है। फिल्म का निर्देशन और नैरोशन ललित मोहन जोशी जी का है। ललित मोहन जोशी कहते हैं कि यह उनकी व्यक्तिगत फिल्म है लेकिन फिल्म को देखकर दर्शक कहेगा कि यह लोक के वैश्विक होने की फिल्म है।
(लेखिका साहित्यिक पत्रिका ‘निकट’ से सम्बद्ध हैं।)