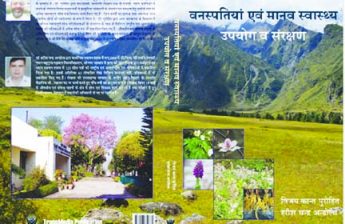पर्यटन किसी भी राज्य के राजस्व के लिए आजीविका का साधन होता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं जो उत्तराखण्ड में अक्सर देखने को मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर इसकी एक बानगीभर हैं। पर्यावरण के लिए खतरा बन चुके प्लास्टिक के ढेरों से हाईकोर्ट तक चिंतित हो चुका है। न्यायालय ने पहाड़ों पर जगह-जगह पड़े प्लास्टिक कचरे से नाराजगी जताते हुए पिछले साल ही सरकार को इसे निस्तारण करने के आदेश दिए थे। हालांकि प्रदेश में पहले से ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 लागू है। बावजूद इसके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए खास उचित उपाय नहीं किए जा सके हैं। आज स्थिति यह है कि प्लास्टिक कचरा पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता पर ग्रहण लगाने के साथ ही प्रकृति के लिए अभिाशप बनता जा रहा है
अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्लास्टिक वेस्ट निस्तारण के लिए सरकार को शीघ्र अधिसूचना जारी करने को कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने भी राज्य में फैले प्लास्टिक वेस्ट पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसके समाधान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर दो सप्ताह में सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कूड़ा वाहनों में जीपीएस टेªकिंग की सुविधा एक माह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है ताकि उसकी समय-समय पर मानिटरिंग की जा सके और कूड़ा वाहनों की लोकेशन का पता लग सके। कोर्ट ने प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में कूडा वाहनों से निर्धारित स्थानों पर कचरा निस्तारण नहीं करने पर भी नाराजगी जताई है। प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 लागू है लेकिन बावजूद इसके गांव- शहर प्लास्टिक से पटे हुए हैं। इसके निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं देती।
दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि उसने प्रदेश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए हर गांव को प्लास्टिक कचरे से मुक्त किया जाना है। प्रदेश के 95 विकासखंडों में कांपेक्टर मशीनें लगाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तक 47 विकासखंडों में इसे लगा देने का दावा है। प्रदेश के 7795 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 16 हजार गांव शीघ्र ही प्लास्टिक कचरे से मुक्त हो जाएंगे। कांपेक्टर मशीन से प्राथमिक निस्तारण होगा उसके बाद इसे हरिद्वार स्थित रिसाइलिंग प्लांट को भेज दिया जाएगा। कचरा उठाने के लिए विकासखंडों को वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त किया जाना है। दावा है कि हर घर में प्लास्टिक कूड़ा उठाने व उसका निपटान की उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 15 वें वित्त आयोग की टाइड निधि में धन की व्यवस्था भी हो गई है। लेकिन इन सबके विपरीत प्रदेश में सभी तरह के कूड़ा निस्तारण की एक तस्वीर यह भी है कि कूड़ा निस्तारण के लिए शहरी निकायों के पास भूमि ही नहीं है वहीं दूसरी ओर कूड़ा प्रबंधन के लिए रिसाइक्लिंग प्लांट की भी भारी कमी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को भी प्रदेश में पंख नहीं लग पाए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में रिसाइक्लिंग प्लांट को मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रदेश के अधिकतर निकायों में हर रोज 2000 टन से अधिक कूड़ा पैदा होता है। इसमें से 26 प्रतिशत कूड़ा अजैविक होता है जिसका निस्तारण करना निकायों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हालात यह हैं कि निकाय क्षेत्र में कई दिनों तक कूड़े का उठान ही नहीं हो पाता है।
अजैविक कचरे की निस्तारण के लिए ठोस व्यवस्था ही नहीं हो पाई है। प्रदेश के संडाध मारते शहरों में लोग जहरीली संास ले रहे हैं। डिस्पोजेबल संस्कृति के चलते भी कूड़े का ढेर लग रहा है। प्रदेश में प्रतिव्यक्ति कूड़ा निकलने का अनुपात बढ़ता जा रहा है। शहर हो या गांव आज भी कूड़ेदानों की कमी दिखती है। राजमार्गों, पार्कों, पर्यटन स्थलों में सही तरह से कूड़ा निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इन जगहों पर कैन या प्लास्टिक की बोतलें यत्र-तत्र बिखरी दिखाई पड़ती हैं। हर शहर व नगर में दुकानदार अपना कूड़ा नालियों में डाल देते हैं। सामूहिक रूप से एक कूड़ेदान खरीदने की तकलीफ नहीं उठाते हैं। प्रदेश के किसी भी शहर में व्यवस्थित टंªचिंग ग्राउंड नहीं है। कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन का प्रयास आधा- अधूरा ही है। गीले व सूखे कचरे के निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। कचरा प्रबंधन के लिए तकनीक का प्रयोग नहीं के बराबर हो रहा है। कचरे को एकत्र करने व उसे प्रोसेस करने के पर्याप्त उपाय नहीं हैं। अपर्याप्त साफ-सफाई और स्वच्छता के चलते कई लोगों की जान चली जाती है। बीमारियां होती हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसका व्यक्ति व राज्य की आर्थिकी पर भी असर पड़ रहा है। प्रदेश में जोशीमठ नगर एक आश जगाता है। जहां पर ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए काम हो रहा है। यहां पर पिछले एक दशक से पालीथिन पर बैन हैं। यहां प्लास्टिक की बोतलें समेत ठोस कूड़े का सेग्रिनेशन और कांपेक्ट कर इसे हरिद्वार स्थित प्लांट में भेज इसका उचित निवारण किया जाता है। इससे नगरपालिका को अच्छी आय भी हो रही है। लेकिन अन्य नगरों में ऐसा नहीं दिखाई देता।
उत्तराखण्ड ही नहीं पूरे देश के कचरा प्रबंधन की स्थिति सही नहीं कही जा सकती। देश में 6.20 करोड़ टन सालाना कचरा पैदा होता है। इसमें से 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 1.7 लाख टन जैव चिकित्सा कचरा, 79 लाख टन खतरनाक अपशिष्ट, 15 लाख टन ई-कचरा, 4.30 करोड़ टन अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा पैदा होने वाला कचरा है। कचरे का प्रबंधन आज तक नहीं हो पाया है। न ही इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। जबकि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। यह नियम कहता है कि व्यक्ति खुद द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली, जलीय क्षेत्रों में नहीं फेंकेगा, न जलाएगा, न ही दबाएगा। व्यक्ति विशेष को छोड़िए नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं भी कचरा निस्तारण नहीं कर पा रही हैं। जबकि कचरे से बिजली, सड़क, सजावटी चीजें बनाई जा सकती हैं। रिड्यूस, रियूज व रिसाइकिल इसका बेहतर विकल्प बन सकती हैं लेकिन जमीन स्तर पर इसके लिए काम नहीं हो पा रहा है। पॉलीथिन और प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। वर्ष 2023 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी प्लास्टिक के प्रदूषण को पराजित करें। भारत की बात करें तो 30 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे का निस्तारण भारत में होता है जबकि 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष निकलता है। देश में लगातार कूड़े का बोझ बढ़ता जा रहा है। विश्व का 13 प्रतिशत कूड़ा भारत में उत्पादित होता है। देश में उत्पादित कूड़े का सिर्फ 28 प्रतिशत ही निस्तारण होता है।
कूड़े में रोजगार: अगर कूड़े को नौकरियों से जोड़े दें तो सत्व कंसल्टिंग व जेपी मार्गन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में ई-कचरा प्रबंधन में 2025 तक पंाच लाख नई नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। भारत सरकार का जोर भी उन क्षेत्रों की तरफ है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और उनमें रोजगार भी हो, इसे ग्रीन जॉब्स नाम दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक देश में 60 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी। इस हिसाब से कुड़ा निस्तारण की चुनौती बढ़ जाती है। एक आंकलन के अनुसार कूड़ा उत्पादन चार प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने का आंकलन है। वर्तमान में देश में कूड़ा बीनने वालों की संख्या डेढ़ से चार लाख के बीच में है। जिसमें से 10 से 25 प्रतिशत ही व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं। बाकी लोग प्रशिक्षण और उपकरणों के अभाव के कारण संक्रामक बीमारियों के जोखिम से भरे रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कूड़ा निस्तारण से जुड़े इन सभी कामगारों को यदि नियोजित कर प्रशिक्षित किया जाय तो न सिर्फ इनके जीवन में सुधार आएगा, बल्कि देश में कूड़ा निस्तारण की क्षमता भी काफी बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि ग्रीन जॉब की सबसे अधिक संभावनाएं ई-कचरा के निस्तारण में है। ई-कचरा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। यह भारत में प्रतिवर्ष 7 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इस समय देश का इलेक्ट्रानिक्स बाजार 7500 करोड़ रुपए का है। यह लगातार बढ़ते जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ ही ई-कचरा बढ़ना भी स्वाभाविक है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में प्रतिवर्ष 20 लाख टन ई-कचरा उत्पादन होगा। वर्तमान में सिर्फ 7.8 लाख टन ई-कचरे का ही रिसाइकलिंग हो रहा है इसमें 10 लाख कर्मचारी जुड़े हैं। जबकि 2025 तक इसमें पांच लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। जरूरी यह है कि ई-कचरे की कंटाई व छंटाई के लिए कुशल व प्रशिक्षित कामगारों की जरूरत है।

ऋषिकेश में गंगा किनारे डम्प कूड़ा
वर्ष 2013 में प्लास्टिक यूज एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नियमावली बनाई गई लेकिन इन नियमों का राज्य में पालन नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम में उत्पादकर्ता, परिवहनकर्ता व विक्रेता की जवाबदेही तय की थी। इसमें निर्माता कंपनी जितना प्लास्टिक निर्मित माल बनाएंगी और विक्रेता जितना बेचेंगे उतना ही खाली प्लास्टिक वापस भी लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो संबधित नगर निकाय का पंचायतों को फंड देंगे, जिससे इसका निस्तारण हो सके। लेकिन प्रदेश में इसका उल्लघंन हो रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में इसके ढेर लग रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना जरूरी है।
जितेंद्र यादव, जनहित याचिकाकर्ता, अल्मोड़ा