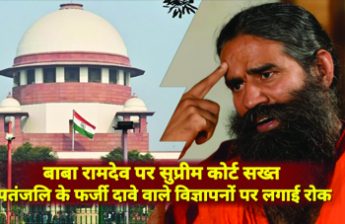अस्सी के दशक की शुरुआत भारतीय लोकतंत्र के लिए नाना प्रकार की समस्या लेकर आई। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस दशक के दौरान अधिकतर ऐसा घटित हुआ, जिसने बतौर राष्ट्र भारत की नींव को खोखला करने का काम किया। इस दशक के पहले पौने पांच साल केंद्र की सत्ता में इंदिरा गांधी काबिज रहीं, तो शेष में उनके पुत्र राजीव गांधी। जनता पार्टी के आंतरिक कलह और कुशासन से त्रस्त होकर देश की सत्ता वापस इंदिरा गांधी के हवाले करने वाली जनता को उम्मीद थी कि आपातकाल के काले अध्याय से सबक लेकर इंदिरा अब सुशासन की नई इबारत लिखने का काम करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संसद सदस्य बन चुके संजय गांधी एक बार फिर से सत्ता का समानांतर केंद्र बनकर उभरने लगे। उनका दखल सरकारी कामकाज में इस कदर बढ़ा कि बहुतों को दोबारा से आपातकाल जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका ने घेर लिया था। वरिष्ठ नौकरशाह पी.सी. एलेक्जेंडर के शब्दों में-
उस दौरान अधिकांश भारतीयों को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी इस दफे प्रशासन को स्वच्छ करने और उसमें नया जोश भरने तथा पारदर्शिता और न्याय स्थापित करने का ईमानदार प्रयास करेंगी, किन्तु इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता संभालने के कुछ माह के भीतर ही भारतीय एवं विदेशी समाचार-पत्रों में सत्ता के एक नए केंद्र के उभरने की खबरें प्रकाशित होने लगीं। संजय गांधी इस समानांतर सत्ता के केंद्र बिंदु बनकर धीरे-धीरे सत्ता पर हावी होने लगे, जिसने उन सभी को बेहद निराश करने का काम किया, जो सत्ता में न रहने के दौरान इंदिरा गांधी के भारी प्रशंसक बन गए थे…जल्द ही नई सरकार ने जनता शासन के पतन के बाद प्राप्त किए अपार सम्मान और सहयोग को खोना शुरू कर दिया।
सत्ता में वापसी के साथ ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल के सभी निशान-प्रमाण मिटाने की कवायद शुरू की। शाह आयोग की जांच रिपोर्ट गायब कर दी गई। जनता सरकार द्वारा गठित की गई विशेष अदालतों को समाप्त करने के साथ-साथ संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल के खिलाफ चल रहे ‘किस्सा कुर्सी का’ मामला भी खत्म कर दिया गया। नौ राज्यों में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की सरकारों को भंग कर वहां दोबारा चुनाव कराने का अलोकतांत्रिक फैसला लेकर इंदिरा गांधी ने आशंकाओं को गहराने का काम किया कि एक बार फिर से वे तानाशाही का मार्ग पकड़ने का मन बना रही हैं। इस दौरान संजय गांधी और उनके करीबियों ने कांग्रेस संगठन और सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का काम किया था। संजय के करीबी नेताओं में अधिकतर युवा थे, जिन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों से कुछ लेना-देना नहीं था। पत्रकार इंदर मेहरोत्रा के शब्दों में-
‘मंदबुद्धि वाले युवा…संसदीय कार्यप्रणाली अथवा विचारधारा अथवा आदर्शवाद से जिनका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था…जो दिमागी तौर पर कमजोर, लेकिन बाहुबली थे। संजय के ये चेले अपनी संसदीय सदस्यता और सत्ता के साथ अपनी निकटता को कम से कम समय में अधिक से अधिक धन कमाने का जरिया मानते थे।’ इंदिरा गांधी सत्ता वापसी के बाद एक बार फिर से आत्ममुग्धता के चरम पर जा पहुंची थी। वे न केवल सनकी मिजाज होने लगी थीं बल्कि बेहद अंधविश्वासी भी हो चली थी। पुपुल जयकर उनके इस आचरण को उनके भीतर कहीं गहरे पसर चुकी असुरक्षा से जोड़कर कर देखती हैं। 16 फरवरी, 1980 को पूर्ण सूर्य ग्रहण था। 84 बरस बाद होने जा रहे इस ग्रहण को लेकर भविष्यवाणियों और अंधविश्वासी बातों से समाचार-पत्र भरे पड़े थे। बकौल पुपुल जयकर इंदिरा इस कदर अंधविश्वासी हो चली थीं कि उन्होंने इस ग्रहणकाल के दौरान अपनी गर्भवती पुत्रवधु मेनका को एक अंधेरे बंद कमरे में रहने के निर्देश दिए थे और स्वयं भी ग्रहण शुरू होते ही अपने कमरे में चली गई थीं और ग्रहण-समाप्ति के बाद ही वे बाहर निकली थीं। जयकर कहती हैं-
‘मैं यह देखकर चकित रह गई कि वे कर्मकांड और अंधविश्वास से किस कदर प्रभावित थीं। आपातकाल के दिनों से उन्हें डराने वाला घातक भय अब भी बना हुआ था। वे किससे डरती थीं? कैसी छाया, कैसा अंधकार उनके साथ चलता था? मैं हैरान थी, लेकिन यह विचार कभी नहीं उठा कि हम मां और बेटे की ‘कयामत की कहानी’ के अंत की ओर बढ़ रहे हैं।’
यह अंत बहुत जल्द आ गया। 23 जून, 1980 की सुबह अमेठी से संसद सदस्य और कांग्रेस के महासचिव संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। संजय स्वयं पायलट थे और उन्हें रोमांचकारी हवाई उड़ान भरने का बेहद शौक था। 23 जून की सुबह वे अपने नए-नवेले दो सीटों वाले छोटे से वायुयान पिट्स एस-2ए में उड़ान भर दिल्ली के खुले आसमान में कलाबाजियों का आनंद ले रहे थे। एक ऐसी ही रोमांचक कलाबाजी के दौरान हवाई जहाज अनियंत्रित होकर सफदरजंग हवाई पट्टी के समीप क्रेश हो गया। इस दुर्घटना में संजय एवं उनके सह-कप्तान की मौत हो गई।
इंदिरा अपने राजनीतिक वारिस की मृत्यु से बेहद टूट गई थीं लेकिन उन्होंने इसका एहसास अपने करीबियों को छोड़कर किसी को होने नहीं दिया। वे संजय गांधी की मृत्यु के मात्र चार दिन बाद ही काम पर लौट आईं। इसके सिवा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। देश में नाना प्रकार की समस्याओं ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ख़तरनाक थीµपंजाबी सूबे में सुलग रही अलगाववाद की चिंगारी, जो आगे चलकर विकराल रूप लेने वाली थी। महाराष्ट्र में श्रमिक असंतोष भी बढ़ने लगा था, जिसका नेतृत्व एक डॉक्टर दत्ता सामंत के हाथों में आने के बाद बम्बई और उसके आस-पास के औद्योगिक इलाकों में सक्रिय मजदूर संगठनों ने बेहतर वेतन और सुविधाओं की अपनी मांग को संगठित तरीके से उठाना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी भी आंदोलन की राह पकड़ने लगे थे, तो बिहार से अलग होकर अपना राज्य मांग रहे छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने भी युवा नेता शिबू सोरेन के नेतृत्व में अपने आंदोलन को धार देना शुरू कर दी थी। पूर्वोत्तर में एक बार फिर से नागा उग्रपंथी अलग राष्ट्र की आवाज बुलंद करने लगे थे। कश्मीर भी एक बार फिर से अलगाववाद की चपेट में आने लगा था।
पंजाब को अलग सिख राष्ट्र बनाए जाने की मांग आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी समय-समय पर सिर उठाते रही है। 1920 में गठित अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन के जरिए 1947 के बाद सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र (खालिस्तान) बनाए जाने की वकालत शुरू कर दी थी। 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने अलगाव की चिंगारी को समय रहते बुझाने की नीयत से सिख बाहुल्य पंजाब प्रदेश के गठन को मंज़ूरी दे हिंदीभाषी इलाकों को अलग कर हरियाणा राज्य बनाया और कुछ हिस्सों को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ दिया था। अविभाजित पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को इस विभाजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान एक केंद्र शासित इकाई बनाते हुए पंजाब और नवगठित हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाए जाने का निर्णय लिया था। सिखों को अपना अलग राज्य तो मिल गया, लेकिन उनके भीतर असंतोष की आग जलती रही, विशेषकर अकाली दल का मानना था कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक बनता है। इसके साथ ही राज्य की तीन प्रमुख नदियों रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भी उसका ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। राज्य के पुनर्गठन के बाद पंजाब के हिस्से इन नदियों का 23 प्रतिशत जल आया था और बाकी पानी से हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की जरूरतों को पूरा किया जाता था।
1972 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में अकाली दल को कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। अपने खोए जनाधार की वापसी और किसी भी कीमत पर राज्य में पुनः सत्ता पाने की नीयत से अकाली दल 1973 में एक विवादित प्रस्ताव लेकर आया, जिसे ‘आनंदपुर साहिब प्रस्ताव’ कहकर पुकारा जाता है। इस प्रस्ताव में चंडीगढ़ को पंजाब को दिए जाने, हरियाणा एवं हिमाचल के पंजाबीभाषी इलाकों को पंजाब में शामिल करने, सिखों को भारतीय सेना में ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने, पंजाब की नदियों के पानी पर पंजाब का हिस्सा बढ़ाने जैसी बुनियादी मांगों के साथ-साथ अलगाववाद की तरफ इशारा करने वाली मांगें भी शामिल थीं। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि संविधान की मूल धारणा के अनुरूप पंजाब को एक स्वायत्त राज्य बनाया जाए जिसमें विदेशी मामलों, रक्षा, मुद्रा, दूरसंचार जैसे कुछ अधिकारों को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में रखते हुए बाकी सभी कामों को राज्य सरकार के अधीन कर दें। प्रस्ताव में ऐसे सभी मसलों पर राज्य सरकार को खुद का कानून बनाए जाने की पूरी छूट दिए जाने की बात भी कही गई थी।
1977 में आपातकाल हटने के बाद राज्य विधानसभा के लिए हुए चुनावों में अकाली दल के हाथों कांग्रेस को भारी हार मिली। अकालियों की सत्ता में वापसी का एक कारण ‘आनंदपुर साहिब प्रस्ताव’ भी रहा था जिसे अब लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। 1977 ही पंजाब की राजनीति को आने वाले समय में गहरा प्रभावित करने वाले शख्स जनरैल सिंह भिंडरावाला का उदयकाल भी रहा। एक जाट सिख परिवार में पैदा हुए जनरैल सिंह की शिक्षा-दीक्षा एक रूढ़िवादी सिख सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन ‘दमदमी टकसाल’ की देख-रेख में हुई थी। इस संगठन का गठन 1706 में सिख गुरु गोविन्द सिंह द्वारा किया गया था। ‘दमदमी टकसाल’ पूर्ण रूप से एक गैर राजनीतिक संगठन था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म का प्रचार एवं गुरु गोविंद सिंह द्वारा बताए मार्ग पर चलकर एक अनुशासित धार्मिक जीवन बिताने की राह प्रशस्त करना था। इसकी अपनी सिख आचार संहिता ‘गुरमत रहत मर्यादा’ है, जिसके अनुसार मांसाहार, मदिरापान, सिगरेट इत्यादि व्यंजनों को प्रतिबंधित माना जाता है।
1977 में जनरैल सिंह को इसी टकसाल का मुखिया चुना गया था। टकसाल का प्रमुख (जत्थेदार) बनने के पश्चात् जनरैल सिंह ने गृहस्थ जीवन त्याग सिख पंथ की सेवा को अपना जीवन-लक्ष्य बना लिया। जनरैल सिंह भिंडरावाला ने सिख धर्म के अनुयायियों को कड़े अनुशासन का जीवन बिताने और सिख पंथ की आचार संहिता का कठोरता से पालन करने के लिए पंजाब के कोने-कोने का दौरा कर एक बड़ा अभियान शुरू करने का काम किया। जल्द ही वह अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में सफल होने लगा था, लेकिन उसने अपने तथा उग्र प्रभावशाली भाषणों के जरिए अपनी छवि एक कट्टरपंथी धर्मगुरु के रूप में तेजी से स्थापित कर डाली थी।
सिख धर्म में पवित्र पुस्तक ‘गुरुग्रंथ साहिब’ को सर्वोच्च माना जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में सिख धर्म के भीतर ही निरंकार सम्प्रदाय की स्थापना हुई, जिसमें जीवित गुरु को सर्वोच्च माने जाने की बात कही गई थी। सिख संत बाबा बूटा सिंह ने इस सम्प्रदाय की नींव रखी थी। धीरे-धीरे यह सम्प्रदाय मुख्य धारा के सिख धर्म से दूर होता चला गया। माना जाता है कि 1977 में अकाली दल के हाथों मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता ज्ञानी जैल सिंह ने संजय गांधी के साथ मिलकर अकालियों की काट करने के लिए भिंडरावाले को राजनीतिक संरक्षण देने की रणनीति बनाई थी। बकौल कैथरीन फैंक- पंजाब में सिख बहुसंख्यकवाद मुखर होने लगा था और उनके राजनीतिक दल अकाली दल ने कांग्रेस को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। फिर 1977 के चुनाव में अकाली दल ने कांग्रेस को हटा दिया। हालांकि इंदिरा सत्ता से बाहर थीं, लेकिन संजय गांधी ने भविष्य के दृष्टिगत राज्य में अकाली दल के प्रमुख को कमजोर करने का फैसला किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें किसी नए व्यक्ति को आगे बढ़ाकर सिखों को विभाजित करने की सलाह दी। ऐसा व्यक्ति, जो अकालियों की खुलकर मुखालफत कर सके। संजय ने अपने कुछ वफादारों को पंजाब में एक नया संत खोजने का काम सौंपा। ऐसा धर्मगुरु, जो सिख एकता को खंडित कर अकाली दल को नुकसान पहुंचा सके। उन्होंने जनरैल सिंह भिंडरावाला नामक दुर्जन खोज निकाला।